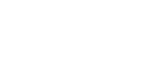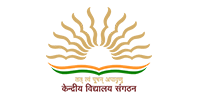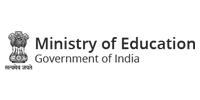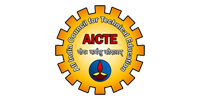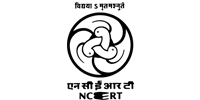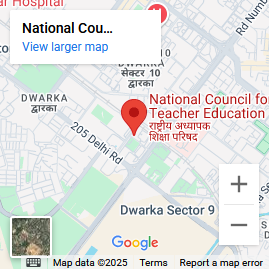परिचय
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और अध्यापक शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव की व्यवस्था करने के अधिदेश के साथ रा.अ.शि.प. अधिनियम, 1993 के अनुसरण में भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में, 17 अगस्त, 1995 को अस्तित्व में आयी थी। यह संगठन एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है और इसमें 4 क्षेत्रीय समितियों जैसे उत्तरी क्षेत्रीय समिति, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के साथ-साथ विभिन्न प्रभाग शामिल हैं जो नई दिल्ली में स्थित हैं। रा.अ.शि.प. द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड), शिक्षा स्नातक (बी.एड), शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड) आदि शामिल हैं। इसमें एनईपी 2020 के अनुरूप नई स्कूल प्रणाली के आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए छात्रों-अध्यापकों का अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल है।
रा.अ.शि.प. को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और इसने विभिन्न राष्ट्रीय अधिदेश जैसे कि एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम) को अपनाया है। रा.अ.शि.प. द्वारा एनईपी 2020 के अनुरूप अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों यानी विनियमन, पाठ्यक्रम और डिजिटल वास्तुकला का संशोधन किया जा रहा है। देश में इस तरह की पहल के साथ रा.अ.शि.प. न केवल अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करती है बल्कि हमारे देश में गुणवत्तायुक्त अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना भी है। एनईपी 2020 में सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा और सेवाकालीन अध्यापक क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ अध्यापकों की भूमिका में आमूल-चूल परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्य
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हे समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं।
परिषद् के कार्य
ऐसे सभी कदम उठाना परिषद् का कर्तव्य होगा क्योंकि वह अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए और अध्यापक शिक्षा के लिए मानकों के निर्धारण और संरक्षण के लिए उपयुक्त हो सकता है और अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू कर सकता है।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करते हैं और उसके परिणाम को पुनः प्रकाशित करते हैं;
- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सिफारिशें करना;
- देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और निगरानी करना;
- स्कूलों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्यापक के रूप में नियोजित होने के लिए न्यूनतम योग्यता या व्यक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करना;
- अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड रखना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और उम्मीदवारों के चयन की विधि, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की सामग्री और पाठ्यक्रम का प्रारूप शामिल हैं;
- नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए, और शारीरिक और निर्देशात्मक सुविधाएं प्रदान करने, स्टाफिंग पैटर्न और कर्मचारियों की योग्यता प्रदान करने के लिए, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों को रखना;
- अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना। इस तरह की परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं में प्रवेश के लिए मानदंड स्थापित करना
- मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क के बारे में दिशानिर्देश देना;
- विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और संचालित करना; अध्यापक शिक्षा और उसके परिणामों का प्रसार;
- समय समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडोंए दिशानिर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और मान्यताप्राप्त संस्थान को उपयुक्त सलाह देना
- मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र विकसित करना;
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएँ बनाना और मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना और अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना;
- अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना; और
- ऐसे अन्य कार्य करते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं।
रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यताप्राप्त कार्यक्रम
निम्नलिखित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए रा.अ.शि.प. ने २८ नवंबर, २०१४ को संशोधित विनियम और मानदंड और मानक अधिसूचित किए:
- बाल-शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम से पूर्वस्कूली शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई)।
- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) ।
- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.)।
- शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम से शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एड.)।
- शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम से शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एड.)।
- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)।
- शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम से शारीरिक शिक्षा में डिग्री (बीपी.एड.)।
- शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपी.एड.)।
- मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.)।
- मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम से शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.)।
- कला शिक्षा (दृश्य कला) में डिप्लोमा कार्यक्रम से कला (दृश्य कला) में स्नातक डिप्लोमा ।
- कला शिक्षा (निष्पादन कला) डिप्लोमा कार्यक्रम से कला (निष्पादन कला) में डिप्लोमा।
- चार वर्षीय समेकित कार्यक्रम द्वारा बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड. डिग्री।
- तीन वर्षीय स्नातक शिक्षा कार्यक्रम (अंशकालीन) द्वारा शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एड.)।
- तीन वर्षीय समेकित कार्यक्रम के माध्यम से बी.एड.,एम.एड. डिग्री (समेकित)।
रा.अ.शि.प. विनियम 2014: हाइलाइट्स
रा.अ.शि.प. ने भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या ३३४ (एफ.एन.ओ. ५१-१ / २०१४ / रा.अ.शि.प. / एनएंडएस) के तहत २८ नवम्बर को १५ कार्यक्रमों के लिए संशोधित नियम २०१४ को संशोधित और अधिसूचित किया। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण पर सरकार द्वारा नियुक्त जस्टिस वर्मा आयोग (जेवीसी)। JVC ने अध्यापक शिक्षा में व्यापक सुधार का सुझाव दिया था जिसे नए विनियम 2014 ने संबोधित किया है। नए नियम रा.अ.शि.प. द्वारा किए गए हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम हैं।
2014 के विनियमों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- 15 कार्यक्रमों के एक विस्तृत पुलिंदे का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पहली बार तीन नए कार्यक्रमों को मान्यता दी गई- चार वर्षीय बी.ए./बी.एससी., बी.एड., तीन वर्षीय बी.एड. (अंशकालीन) और तीन वर्षीय बी.एड.-एम.एड. कार्यक्रम।
- तीन कार्यक्रमों की अवधि- बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड.- दो साल के लिए बढ़ा दी गई है तथा इन्हें और अधिक व्यावसायिक रूप से सशक्त एवं सर्वात्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल बनाया गया है।
- अब एकल संस्थानों के स्थान पर अध्यापक शिक्षा को समग्र संस्थानों के रूप में (बहु-विषयक या बहु-अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- क्रमानुसार प्रत्येक पाठयक्रम में तीन घटक हैं-सिद्धांत, अभ्यास और इंटर्नशिप इसमें शमिल हैं तथा कम-से-कम 25 प्रतिशत कार्यक्रमों को स्कूल आधारित कार्यकलापों और इंटर्नशिप के लिए विकसित किया गया है।
- आईसीटी, योग शिक्षा, लैंगिक और विकलांगता/समावेशी शिक्षा प्रत्येक कार्यक्रम व पाठयक्रम का अंभिन्न अंग हैं।
- अधिक एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- अध्यापक प्रशिक्षक एम.एड. डिग्री प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ होती है।
- अध्यापक प्रशिक्षक मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण (ओडीएल) अन्तर्निहित गुणवत्ता सुनिश्चित प्रद्धति के साथ अधिक मजबूत हो गया है।
- सेवारत शिक्षकों के पास उच्च अध्यापक शिक्षा योग्यता डी.एल.एड. (ओडीएल), बी.एड. प्राप्त करने के अधिक विकल्प हैं।
- आवेदन करते समय संबद्ध विश्वविद्यालय/निकाय से एनओसी अनिवार्य है।
- निरीक्षण/निगरानी के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारदर्शी उपयोग के लिए आवेदन का प्रावधान, शुल्क का भुगतान, टीम के दौरे की रिपोर्ट आदि ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत किया गया है। (इसके लिए] ई.शासन अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है)।
- प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान को रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी से प्रत्येक 5 वर्षों में अनिवार्य मान्यता प्राप्त करनी होती है। (इस संबंध में पहले ही एनएएसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं)